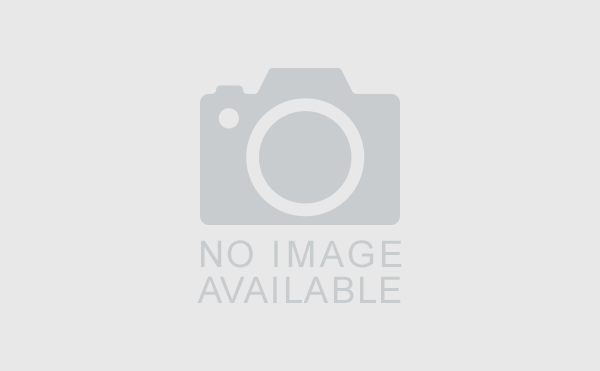राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा ऐतिहासिक संदर्भ, विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति को लेकर उठाए 14 सवाल
नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक दुर्लभ कदम उठाते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कानूनी राय मांगी है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति देने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
क्या है अनुच्छेद 143(1)?
संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। इस संदर्भ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को एक संविधान पीठ गठित करनी होगी, जो इन सवालों का जवाब देगी।
राष्ट्रपति ने उठाए 14 अहम सवाल
राष्ट्रपति मुर्मू ने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधेयकों पर सहमति नहीं दी जाती है, तो इसे ‘मानी हुई सहमति’ (Deemed Assent) माना जाएगा। राष्ट्रपति ने इसे संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया है और कहा है कि यह प्रावधान राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करता है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं:
-
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत होने पर उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
-
क्या राज्यपाल, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं?
-
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा समीक्षा योग्य है?
-
क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
-
अगर संविधान में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेशों द्वारा राज्यपाल के निर्णय की समय-सीमा तय की जा सकती है?
-
क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा समीक्षा योग्य है?
-
अगर संविधान में कोई समय-सीमा नहीं है, तो क्या न्यायालय समय-सीमा निर्धारित कर सकता है?
-
क्या राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेना आवश्यक है?
-
अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून बनने से पहले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं?
-
क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक आदेशों को बदला जा सकता है?
-
क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक, राज्यपाल की सहमति के बिना कानून बन सकता है?
-
क्या अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक व्याख्या के मामलों को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजना अनिवार्य है?
-
अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या केवल प्रक्रिया संबंधी मामलों तक सीमित हैं या वे संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत भी आदेश जारी कर सकती हैं?
-
क्या संविधान के तहत संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अनुच्छेद 131 के अलावा कोई अन्य उपाय है?
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल को विधेयकों पर सहमति देने की एक निश्चित समय-सीमा में निर्णय लेना होगा। अगर इस समय-सीमा का पालन नहीं होता है, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि भले ही अनुच्छेद 200 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसे इस प्रकार नहीं समझा जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक पर निर्णय न लें।
इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, और अगर इस अवधि से अधिक समय लगता है, तो इसके स्पष्ट कारण राज्य सरकार को बताने होंगे।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आए इस फैसले की आलोचना कई नेताओं ने की थी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल थे। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, “राष्ट्रपति को एक निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। क्या अब जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका के कार्य करेंगे, और संसद का भी काम संभालेंगे?”
आगे की राह
अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वह राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों का क्या जवाब देती है। अगर अदालत इस पर संविधान पीठ का गठन करती है, तो यह भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।